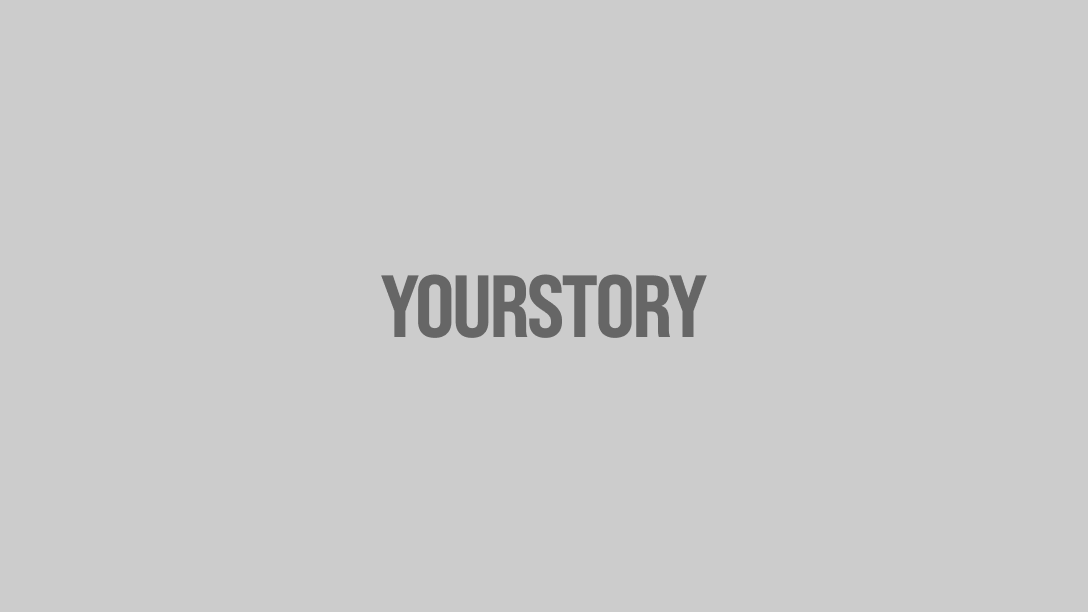शहरों को उपजाना होगा अपना खुद का अन्न
खाद्य संकट एक बड़ी समस्या...
शहरों या शहर से सटे इलाकों में कृषि उत्पादों के उत्पादन को किसानों की भाषा में पेरी-अर्बन (शहर से सटे इलाकों) कृषि कहा जाता है और मौजूदा वक्त में दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है।

पेरी अर्बन फार्मिंग (सांकेतिक तस्वीर, साभार- सोशल मीडिया)
खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी के लिए पौष्टिक और प्रोटीन की भरपूर मात्रा वाले उत्पाद जैसे अनाज, सब्जियां, फल, दूध, अण्डे, मांस और मछली के ऊंचे दाम जिम्मेदार हैं।
शहर के नजदीक होने के कारण आपूर्ति की समस्या दूर करने और इनकी कीमतों को काबू करने के लिए इन उत्पादों को ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।
यह तय मानिये कि जनसंख्या ही बढ़ेगी, जमीन नहीं फिर खेती वाली जमीन तो हर हाल में घटेगी ही। कुछ आभासी विकास के नाम पर हथिया ली जायेगी, कुछ वास्तविक विकास की बलिवेदी चढ़ेगी जो बचेगी उसे शहरीकरण लील जायेगा। यह भी निश्चित है कि भविष्य में शहरों को मजबूरन ही सही अपना खाना खुद उपजाना होगा। भविष्य की शहरी खेती के इस रीति का नाम है पेरी-अर्बन फार्मिंग। शहरों या शहर से सटे इलाकों में कृषि उत्पादों के उत्पादन को किसानों की भाषा में पेरी-अर्बन (शहर से सटे इलाकों) कृषि कहा जाता है और मौजूदा वक्त में दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि कुछ देशों में तो इसे शहरी योजना का हिस्सा बना लिया गया है। इस प्रकार की खेती के अनगिनत लाभ हैं और यह पर्यावरण के लिए लाभदायक होने के साथ ही खेतों से आने वाली ताजा फसल की आपूर्ति भी बढ़ाती है।
खाद्य पदार्थों के दाम में आने वाली जबरदस्त तेजी पर काबू पाने के लिए भारत भी अपनी लम्बी अवधि की नीतियों में इसे शामिल कर ये लाभ उठा सकता है। इस तरह की खेती की आवश्यकता बढ़ रही है। पहली बात यह कि खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी के लिए पौष्टिक और प्रोटीन की भरपूर मात्रा वाले उत्पाद जैसे अनाज, सब्जियां, फल, दूध, अण्डे, मांस और मछली के ऊंचे दाम जिम्मेदार हैं। दूसरी बात यह कि शहरी इलाकों में इन खाद्यान्नों की मांग तुलनात्मक रूप से काफी तेजी से बढ़ रही है। और तीसरी बात इनमें से सभी उत्पाद ऐसे हैं, जिनका उत्पादन शहर या उसके आसपास के इलाके में आसानी से किया जा सकता है। शहर के नजदीक होने के कारण आपूर्ति की समस्या दूर करने और इनकी कीमतों को काबू करने के लिए इन उत्पादों को ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।
शहरों में छोटे पैमाने पर होने वाली खेती जैसे रसोई के बाहर और छत पर बगीचा बनाना, मकानों के पिछले हिस्से में पशुपालन करना भी शहरी और पेरी-अर्बन खेती का ही एक रूप है और इसे प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हालांकि इसका दायरा सीमित है विशेष तौर पर गहन आबादी वाले शहरों में, जहां जमीन की उपलब्धता के अभाव में बहुमंजिले अपार्टमेंट की संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। इस तरह की इमारतों में रहने वालों के लिए खुली जगह सिर्फ बालकनी ही होती है। हालांकि शहरों के बाहर कुछ इलाकों को पेरी-अर्बन खेती, बागवानी और पशु पालन के लिए चुना जा सकता है।
मुंबई के उपनगरीय इलाकों में कई लोग छोटे-छोटे भूखण्ड़ों पर खेती कर बिना फर्टिलाइजर और कीटनाशक का प्रयोग किये ऑर्गेनिक फल-सब्जियां उगा रहे हैं। ये अपनी उपज को मुंबई तथा नजदीकी बाजार में बेच रहे हैं। दिल्ली में यमुना के किनारे और आसापास बड़े पैमाने पर सब्जियां उगायी जाती रही हैं। दिल्ली के ही जनकपुरी में लोग छतों पर सब्जियां उगा रहे हैं और इलाके के कई हिस्से में लोग अपने घरों की छतों पर किचन गार्डन बना रहे हैं। हौजखास, वसंत कुंज, गुलमोहर पार्क, वसंत विहार के अलावा उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में भी ऐसा दिखने लगा है। लखनऊ और कानपुर में भी लोग नींबू, टमाटर, धनिया, बैंगन, भिण्डी, शिमला मिर्च, मिर्च, तोरई, लौकी, सीताफल, टिण्डा, पुदीना, करेला, लोबिया, गोभी, चौलाई, ब्रोकली, सेम, पालक, जैसी सब्जियां लोग खुद ही उगा और खा रहे हैं।
दिल्ली में एक संस्था लोगों को यह बताती है कि कैसे आप अपने जरूरत भर की सब्जियां अपनी छत या मकान के खाली जगह का उपयोग कर उगा सकते हैं। हालांकि इस तरह की कई कोशिशें महज रासायनिक खादों, ऑक्सीटोसिन और कीटनाशक वाले रसायनों तथा सीवर के गंदे पानी से सिंचित और धोयी गयी सब्जियों से बचने और ऑर्गेनिक फूड के फैशन तथा उसके बढ़ते बाजार के मद्देनजर किया जा रहा है। कुछ लोग सब्जियों के बढ़े दामों या अपने शौक के चलते भी ऐसा करते रहे हैं। लखनऊ की सीमा से लगे कई सीमांत क्षेत्र हैं, जहां खेती-बाड़ी के लिए पर्याप्त जमीन है। आखिरकार इस जमीन का इस्तेमाल कम मूल्य वाले अनाज उगाने के लिए क्यों किया जाय, जबकि इन अनाजों को कहीं और भी उगाया जा सकता है? यह बात पूरे राजकीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होती है, जहां शहरों और कस्बों से ऐसे इलाके सटे हैं, जिनकी जमीन खेती के लिए काफी उपजाऊ है।
इस क्षेत्र के प्रगतिशील किसान ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अनाज के बजाय अधिक मूल्य वाले बागवानी या प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं। ये किसान मवेशी उत्पाद कीमत के लिहाज से आकर्षक हो चुके शहरों में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अन्य महानगरों, शहरों और छोटे कस्बों की परिस्थितियां ज्यादा भिन्न नहीं हैं। कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने शहरी और पेरी-अर्बन खेती पर एक नीतिगत दस्तावेज (संख्या 67) पेश किया है। इस दस्तावेज में अकादमी ने ऐसी खेती को शहरी भूमि इस्तेमाल योजना और राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनायें जाने की सिफारिश की है।
फिलहाल पेरी-अर्बन खेती में मौजूद असीम संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए न तो शहरी और न ही ग्रामीण योजना में कुछ प्रावधान किये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने भी शहरों की खाद्य पदार्थों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें हरा-भरा बनाये रखने में पेरी-अर्बन खेती की महत्वपूर्ण भूमिका बतायी है। एफएओ ने तो सदस्य देशों से इस किस्म की खेती को कृषि व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाने का सुझाव दिया है।
शहरी और पेरी-अर्बन खेती को बढ़ावा देने की औपचारिक शुरुआत 2011 में 'वेजिटेबल इनीशिएटिव इन अर्बन क्लस्टर्सÓ योजना के साथ हुई थी। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों की संख्या घटाकर शहरी आबादी को किफायती कीमत पर अच्छी गुणवत्ता की ताजी और प्रसंस्कृत सब्जियों की आपूर्ति करना था। इस योजना को कुछ क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया था और वहां मिले संतोषजनक नतीजों को देखते हुए इसे अन्य शहरों में भी लागू करने की सलाह दी जा सकती है।
पर्यावरणविद मानते हैं कि इससे शहरों के हरित क्षेत्र में इजाफा होगा और प्रदूषण भी कम होगा। घरों से निकला कार्बनिक कचरा इन खेतों में खाद के रूप में निपट जायेगा। यह खाद्य चक्र बदलेगा तो लोगों को स्वास्थ्यप्रद खाद्य सामग्री आसानी से और अपेक्षाकृत कम दाम में मुहैया हो सकेगी तथा हर उम्र के लोगों को काम मिलेगा तथा आजीविका का अतिरिक्त साधन भी। इस शहरी खेती में छोटे उद्यमी शामिल होंगे तो बड़ी कंपनियां भी इससे जुड़ेंगी जो उपजे उत्पाद को सोशल मीडिया और एप्स के जरिये थोक में शहरी रेस्टोरेंट और फुटकर में सीधे ग्राहकों से संपर्क कर बेचेंगी, कोई बिचौलिया नहीं होगा तो ये सस्ती मिलेंगी।
फूड डेवलपर ग्राहकों से साप्ताहिक आपूर्ति का समझौता और फार्मिंग करने वाली कम्पनियों में हिस्सेदारी के लिए छोटे उद्यमी क्राउड फंडिंग का सहारा लेंगे। पब्लिक-प्राइवेट मॉडल भी इस क्षेत्र में फले फूलेगा। लोग अपनी छतों, खाली जगहों को फार्मिंग के लिए किराये पर देंगे तथा राज्य और केंद्र सरकारें इसके प्रोत्साहन के लिए नए-नए उपक्रम चलायेंगी। हालांकि पेरी-अर्बन खेती में कुछ सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान इस कृषि के कारण सम्भावित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है।
अक्सर ऐसे इलाकों में खेती के लिए किसान आसानी से उपलब्ध गटर का पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई हानिकारक प्रदूषक तत्व मौजूद होते हैं। इस तरह की समस्या का सबसे बड़ा उदाहरण है मुम्बई, जहां पेरी-अर्बन खेती में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। मुंबई के बाजार में आने वाली करीब 20 फीसदी हरी सब्जियां रेल की पटरियों के किनारे मौजूद गंदगी में उगायी जाती हैं। पटरियों के किनारे पड़ा यह कचरा अशोधित होता है, जिसमें बड़ी मात्रा में हानिकारिक जीवाणु और नाइट्रेट जैसे प्रदूषक मौजूद होते हैं।
इसलिए रेल की पटरियों के किनारे उगायी जाने वाली सब्जियां प्रदूषित होती हैं। स्थानीय निकायों के लिए जरूरी है कि वे गटर के पानी को खेती के इस्तेमाल की खातिर छोडऩे से पहले शोधन करें। इसके अतिरिक्त शहरी इलाकों में बीज, पौधे और खाद्य एवं उर्वरकों अन्य कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे लोग ऐसी खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। इसके अतिरिक्त किसानों को कुछ तकनीकी जानकारी और मशरूम या अन्य महंगी सब्जियां उगाने का प्रशिक्षण देने की भी दरकार होगी।
यह भी पढ़ें: हिंदू कैंसर मरीज के लिए पैसे जुटाने के लिए नहीं निकाला बंगाल के मुस्लिमों ने मुहर्रम जुलूस